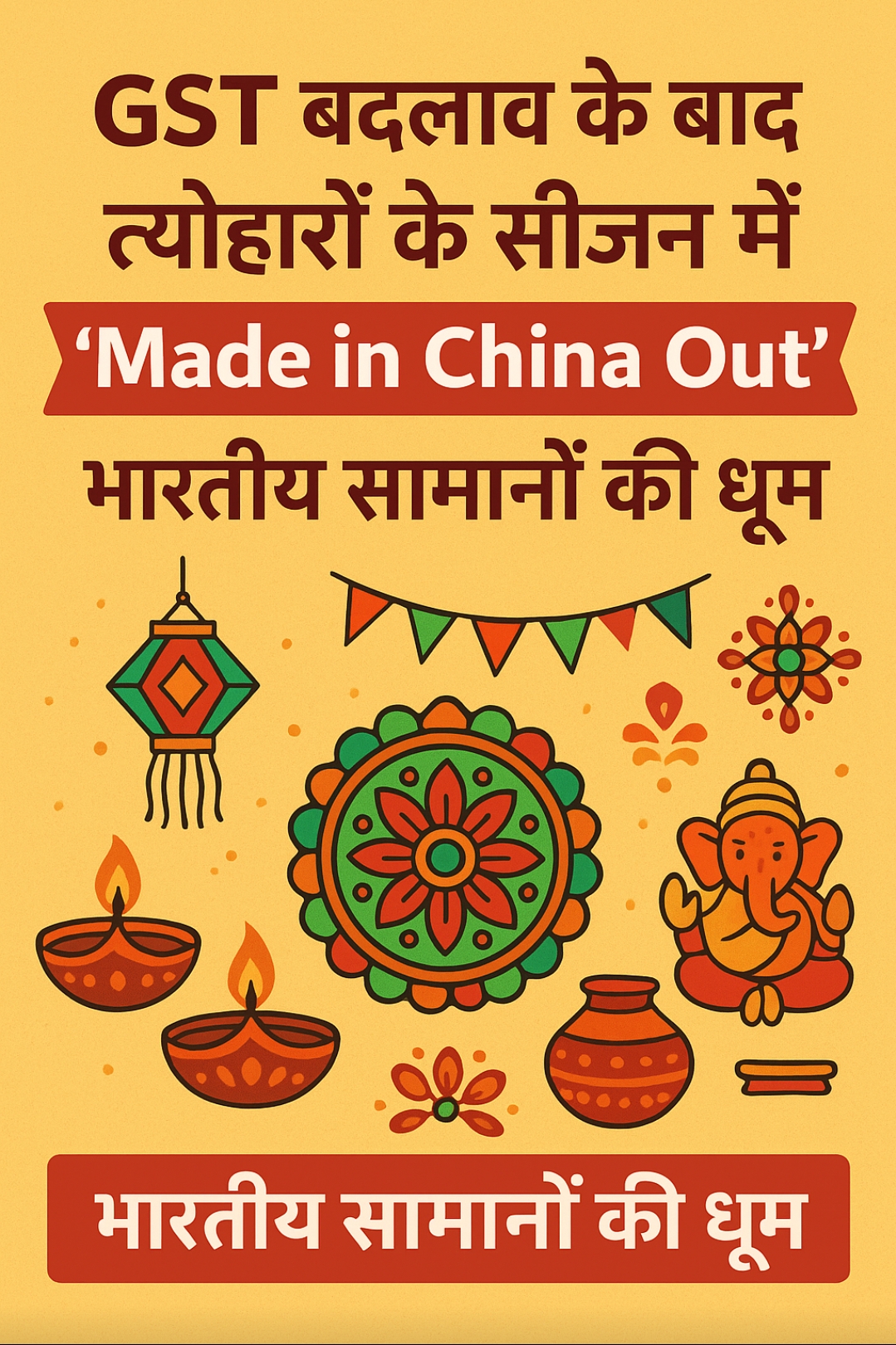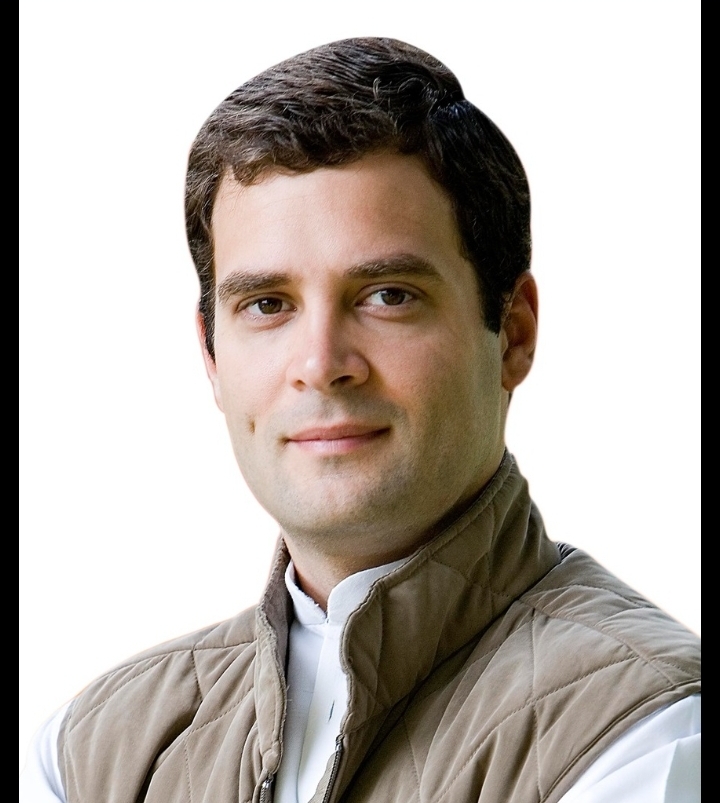भारतीय राजनीति में धर्म आधारित व्यवस्था का प्रयोग

भारत एक ऐसा देश है जिसकी आत्मा विविध धार्मिक विचारों, आस्थाओं और मान्यताओं में रची-बसी है। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और अनेक आदिवासी धार्मिक परंपराएं सह-अस्तित्व में रहती आई हैं। यही विविधता भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को गहराई प्रदान करती है। किंतु जब राजनीति और धर्म का मेल गहरा होने लगता है, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक हो जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में धर्म का स्थान क्या होना चाहिए। भारत जैसे बहु-धार्मिक समाज में यह बहस और भी जटिल हो जाती है कि क्या राजनीति को धर्म से प्रेरणा लेनी चाहिए, या पूर्णत: धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए।
इस सम्पादकीय लेख में हम भारतीय राजनीति में धर्म आधारित व्यवस्था के इतिहास, विकास, चुनौतियों और संभावनाओं की गहन समीक्षा करेंगे।
भारतीय राजनीति और धर्म का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
भारत में धर्म और राज्य व्यवस्था का रिश्ता प्राचीन काल से ही देखा जा सकता है। वैदिक काल में राजा को धर्मराज्य की रक्षा करने वाला माना जाता था। धर्म का आशय यहां केवल पूजा-पाठ या आस्था से नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था के आदर्श सिद्धांतों से था। रामराज्य का आदर्श भी इसी “धर्म आधारित शासन” की व्याख्या प्रस्तुत करता है।
मौर्य और गुप्तकाल में धर्म का असर राजनीति में विद्यमान रहा, किंतु अशोक ने राजनीति को अहिंसा और बौद्ध धर्म की करुणा से जोड़कर एक अलग उदाहरण प्रस्तुत किया। मध्यकाल में इस्लामी शासकों ने अपनी धार्मिक पहचान और कानूनों को प्रशासन में शामिल किया। उदाहरण स्वरूप, दिल्ली सल्तनत और मुगलकालीन राजनीति धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक आधार पर शासन के बीच झूलती रही। अकबर द्वारा दीन-ए-इलाही जैसी पहल से धार्मिक सहिष्णुता को शासन की बुनियाद बनाने का प्रयास किया गया।
ब्रिटिश शासन में “विभाजित करो और राज करो” नीति ने राजनीति में धर्म की भूमिका को नया रूप दिया। 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधार से अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई, जिसने भारतीय राजनीति में धर्म आधारित पहचान को औपचारिक रूप से संस्थागत कर दिया। यही बीज आगे चलकर देश के विभाजन का कारण बने।
संविधान और धर्मनिरपेक्षता
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इतने विविध धार्मिक समाज को लोकतांत्रिक और समान नागरिक अधिकारों वाली रूपरेखा में कैसे समाहित किया जाए।
संविधान की प्रस्तावना में भारत को “धर्मनिरपेक्ष” राष्ट्र घोषित किया गया। अनुच्छेद 25 से 28 ने प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता, पूजा और प्रचार का अधिकार दिया। लेकिन यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की सीमाओं में बंधी रही। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिम की सेक्युलरिज़्म की तरह धर्म और राज्य को पूर्णत: अलग नहीं करती, बल्कि “सर्व धर्म सम भाव” की अवधारणा को स्वीकार करती है।
संविधान स्पष्ट करता है कि राज्य किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं देगा, लेकिन सभी धर्मों का समान सम्मान करेगा। यही भारतीय “धर्मनिरपेक्षता” की विशेषता है, जिसकी वजह से भारत में धर्म आधारित राजनीति संवेदनशील विषय बनी रहती है।
स्वतंत्र भारत में धर्म आधारित राजनीति
1. विभाजन की स्मृति और मुस्लिम राजनीति
1947 के विभाजन ने भारत में मुस्लिम पहचान की राजनीति को गहरा आघात पहुंचाया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई, किंतु भारत में मुस्लिम राजनीति छोटे-छोटे क्षेत्रीय दलों और नेताओं तक सीमित रह गई।
2. कांग्रेस और धर्म का संतुलन
कांग्रेस ने खुद को धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि चुनावी राजनीति में कांग्रेस ने समय-समय पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों समुदायों की भावनाओं को संतुलित कर वोट बैंक साधने की रणनीति अपनाई। इसे अक्सर “तुष्टिकरण की राजनीति” कहा गया है।
3. जनसंघ, भाजपा और हिन्दुत्व
1951 में भारतीय जनसंघ, और बाद में भाजपा ने हिंदुत्व विचारधारा को राजनीतिक आधार बनाया। अयोध्या आंदोलन और राम जन्मभूमि विवाद भारतीय राजनीति का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ। भाजपा का उभार इस तथ्य को दर्शाता है कि धर्म, खासकर बहुसंख्यक धर्म, भारतीय लोकतंत्र में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।
4. क्षेत्रीय दल और धार्मिक पहचान
पंजाब में अकाली दल, जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, दक्षिण भारत में द्रविड़ दल, सभी ने अपनी-अपनी धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान को राजनीति से जोड़ा।
धर्म आधारित व्यवस्था के सकारात्मक पहलू
बहस का यह पक्ष अक्सर अनदेखा रह जाता है कि धर्म आधारित राजनीति के कुछ सकारात्मक निहितार्थ भी हो सकते हैं।
- धार्मिक मूल्य जैसे न्याय, करुणा, समानता और सेवा राजनीति में नैतिकता ला सकते हैं।
- राजनीति में धार्मिक सहभागिता सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत कर सकती है।
- भारत जैसे धार्मिक राष्ट्र में पूरी तरह धर्म से दूरी बनाना व्यावहारिक रूप से कठिन है; जनता की आस्थाएं नीतियों पर असर डालती ही हैं।
- कई बार धार्मिक संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसेवा में सरकार से भी अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
धर्म आधारित व्यवस्था की चुनौतियां
हालांकि इसके दुष्परिणाम कहीं अधिक गंभीर माने जाते हैं:
- सांप्रदायिकता और विभाजन: धर्म आधारित राजनीति अक्सर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक को आमने-सामने खड़ा कर देती है।
- लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास: राजनीति का मूल आधार नागरिकता होनी चाहिए, न कि धार्मिक पहचान।
- महिला अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार: धर्म आधारित कानून प्रायः व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करते हैं, जैसे तीन तलाक या समान नागरिक संहिता की बहस।
- वोट बैंक राजनीति: धर्म आधारित अपील लोकतंत्र को मुद्दों से भटका कर भावनाओं पर केंद्रित कर देती है।
- राष्ट्रवाद बनाम धार्मिक राष्ट्र: क्या भारत राष्ट्र-राज्य के बजाय धार्मिक राज्य बन सकता है? यह प्रश्न लोकतंत्र के भविष्य के लिए गंभीर है।
धर्म और राजनीति पर न्यायपालिका की स्थिति
सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार स्पष्ट किया है कि राजनीति में धर्म के अंधाधुंध उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने “हिंदुत्व” को जीवन पद्धति बताया, लेकिन इसे राजनीतिक हथियार बनाने की सीमाएं भी रेखांकित कीं। 2017 में अदालत ने कहा कि धर्म, जाति या भाषा के आधार पर वोट मांगना जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है।
समकालीन परिदृश्य
21वीं सदी में धार्मिक राष्ट्रीयता भारतीय राजनीति की केंद्रीय धारा बन चुकी है। भाजपा ने भारतीय समाज में हिंदुत्व को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में स्थापित किया है। वहीं विपक्षी दल अक्सर धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने और तुष्टिकरण की राजनीति छोड़ने के दबाव में हैं।
अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षा और प्रतिनिधित्व की कमी की भावना से जूझ रहे हैं। दूसरी ओर, बहुसंख्यक समुदाय का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि उसके धार्मिक अधिकार अब तक दबाए गए थे। इस द्वंद्व ने भारतीय लोकतंत्र को नए संकट के सामने खड़ा कर दिया है।
क्या होना चाहिए आगे का रास्ता?
- समान नागरिक संहिता पर सहमति ढूंढी जाए ताकि धर्म आधारित पर्सनल लॉ समाज को विभाजित न करें।
- धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाए जिससे नई पीढ़ी लोकतांत्रिक और तर्कशील सोच के साथ आगे बढ़े।
- धार्मिक संवाद और सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया जाए; भारत का भविष्य सभी धर्मों की साझी संस्कृति पर टिका है।
- कानून और न्यायपालिका की भूमिका स्वतंत्र और कठोर रहनी चाहिए ताकि कोई दल धार्मिक भावनाओं का घोर दुरुपयोग न कर सके।
- जन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए—रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक न्याय को चुनावी विमर्श का केंद्र बनाना आवश्यक है।
निष्कर्ष
भारतीय राजनीति में धर्म आधारित व्यवस्था स्थायी विषय है, जो न तो पूरी तरह गायब हो सकती है और न ही पूरी ताकत से लागू हो सकती है। भारत की ताकत उसकी विविधता और सहिष्णुता में है। यदि धर्म आधारित राजनीति को नियंत्रित ढंग से लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ संतुलित रखा जाए, तो यह सामाजिक नैतिकता और जनकल्याण का साधन बन सकती है। लेकिन यदि यह सांप्रदायिकता, भेदभाव और बहिष्करण में बदल जाए, तो यह भारत की एकता और लोकतंत्र दोनों के लिए खतरा बन जाती है।
भारत का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि क्या वह धर्म को राजनीति का उपकरण बनने देगा या उसे केवल नैतिक प्रेरणा स्रोत के रूप में सीमित रखेगा। भारत को चाहिए कि वह संविधान और “सर्व धर्म सम भाव” की नींव पर टिके रहते हुए धर्म और राजनीति के संतुलन का मार्ग खोजे।