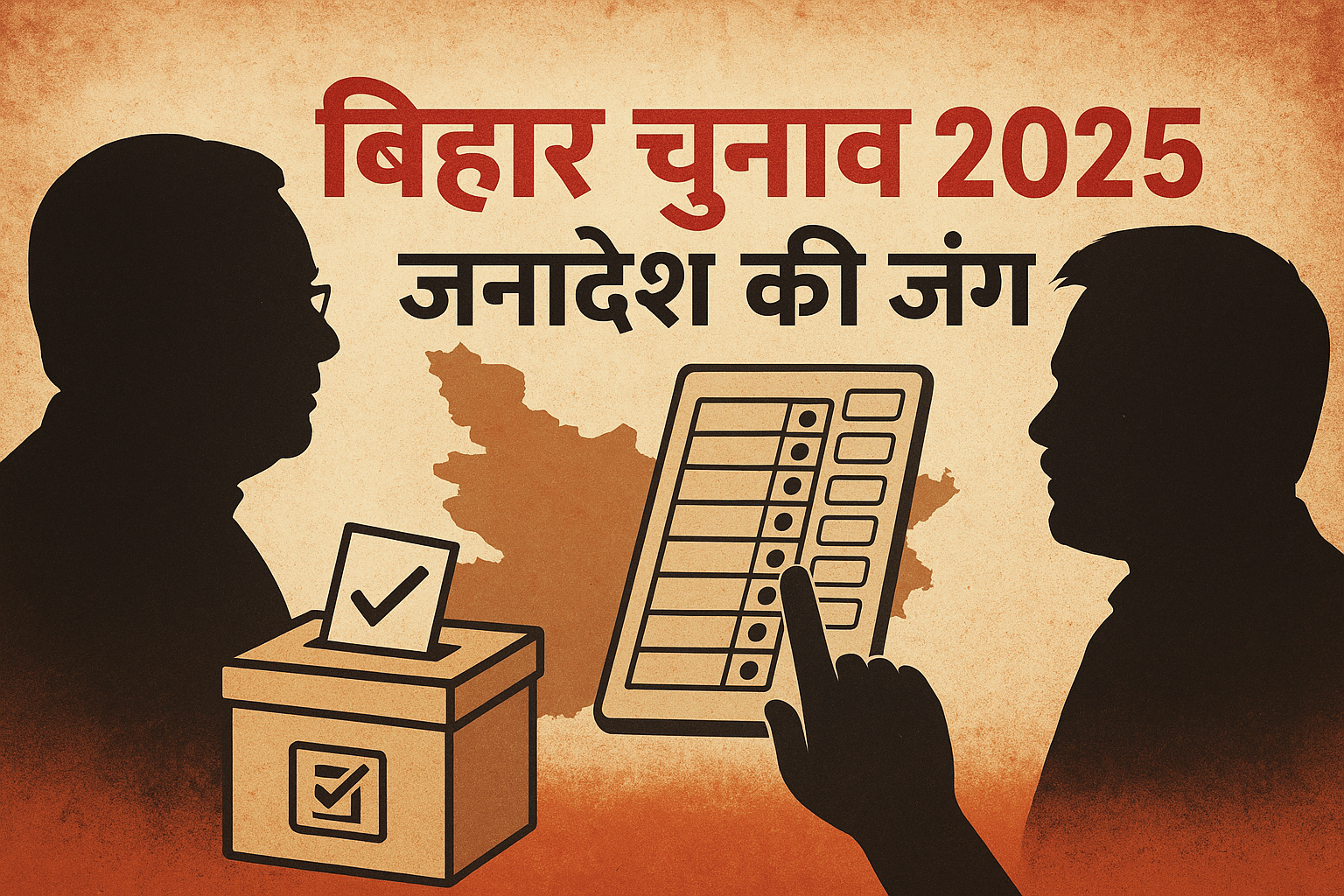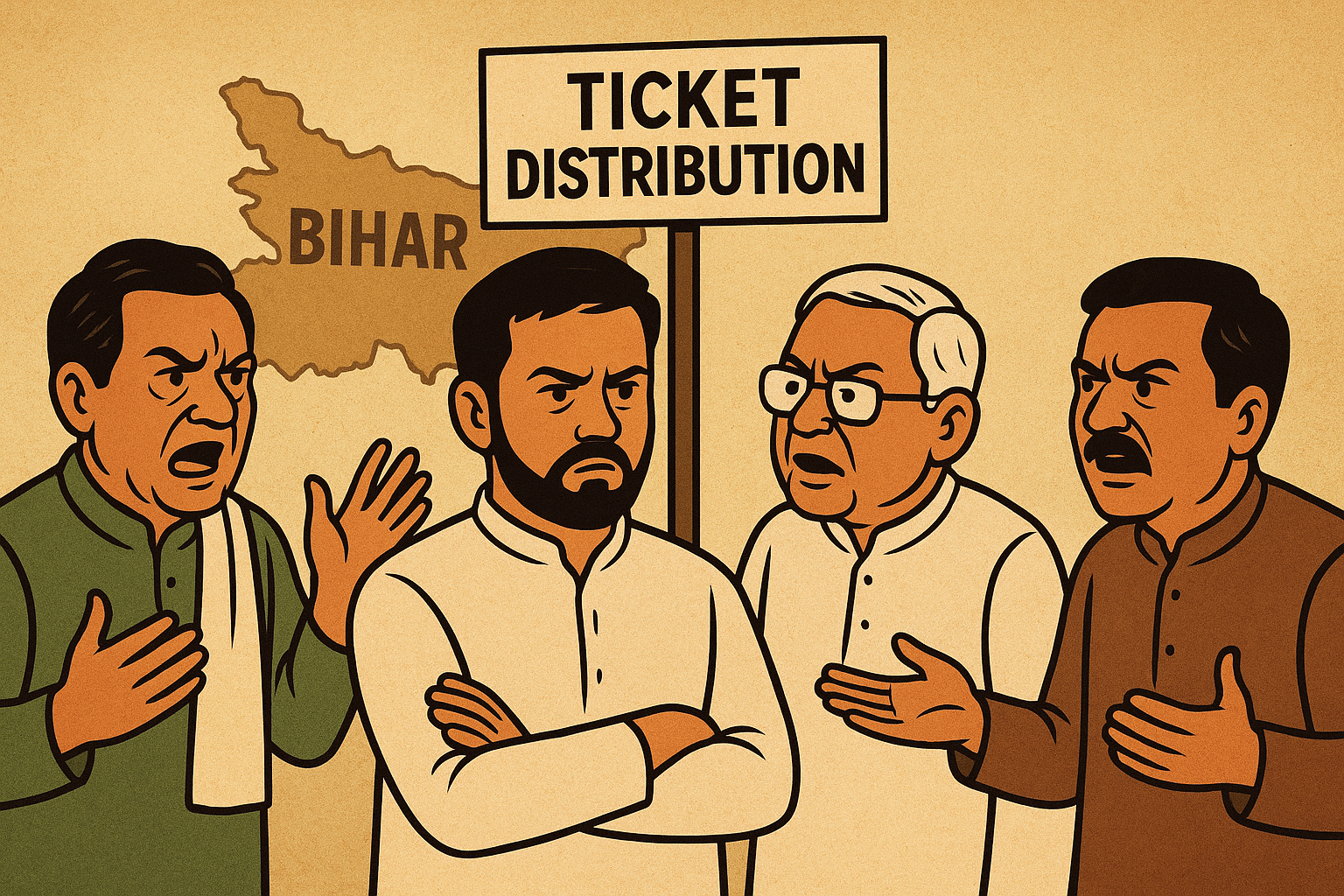**“सत्ता नहीं, सेवा हो राजनीति का मूल मंत्र”**
भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की विशेषता रही है कि यहां राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं बल्कि लोकसेवा का माध्यम मानी जाती थी। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज़ादी के शुरुआती दशकों तक राजनीति एक आदर्श, समर्पण और त्याग का पर्याय थी। गांधीजी के सत्य और अहिंसा के मार्ग, नेहरू और पटेल का राष्ट्रनिर्माण का दृष्टिकोण, लोहिया की समाजवादी सोच और अटल बिहारी वाजपेयी का उदात्त व्यवहार — इन सबके कारण जनता राजनीति को श्रद्धा और विश्वास की नज़र से देखती थी। मगर आज स्थिति बदल चुकी है। राजनीति आदर्शवाद से अवसरवाद की ओर गिरी है, और नेताओं के आचरण ने लोकतंत्र की बुनियाद को हिला दिया है।
गिरावट की तस्वीर
संसद और विधानसभाओं का हाल किसी माननीय चर्चा मंच से अधिक किसी शोरगुल वाले अखाड़े जैसा नजर आता है। जहाँ एक समय नीति-निर्माण और रचनात्मक बहस होती थी, वहीं आज आरोप-प्रत्यारोप, असंसदीय भाषा और व्यक्तिगत हमले आम हो चुके हैं। कई बार सत्र बाधित होते रहते हैं और महत्वपूर्ण विधेयक शोर-शराबे के बीच पारित कर दिए जाते हैं, जिससे लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप प्रभावित होता है।
चुनावी राजनीति में भी गिरावट साफ दिखती है। रैलियों और भाषणों में जनता के मूल मुद्दे – शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्या, बेरोजगारी – गौण हो जाते हैं। नेताओं का ध्यान जातीय समीकरणों, धार्मिक ध्रुवीकरण और विरोधियों को नीचा दिखाने पर केंद्रित रहता है। चुनाव धनबल और बाहुबल के बिना जीतना कठिन दिखता है, जिससे ईमानदार और योग्य लोग राजनीति में आना ही नहीं चाहते।
जनता और लोकतंत्र पर असर
नेताओं के आचरण की यह गिरावट सीधा प्रभाव जनता पर डालती है। लोकतंत्र का आधार विश्वास और भागीदारी है, लेकिन जब जनता देखती है कि उसके प्रतिनिधि निजी हित साधने में लगे हैं, तो राजनीतिक व्यवस्था पर से भरोसा उठ जाता है। युवाओं में राजनीति के प्रति निराशा और उदासीनता बढ़ रही है। वे राजनीति को केवल सत्ता का खेल मानते हैं, जो लोकतांत्रिक भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है। मूल मूल कारण
इस स्थिति के पीछे कई प्रमुख कारण हैं:
– राजनीति में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार का बढ़ता प्रभाव।
– चुनावों में बेहिसाब खर्च और धनबल का बोलबाला।
– वैचारिक राजनीति का लोप और अवसरवाद का बढ़ना।
– मीडिया और सोशल मीडिया में सनसनी पर ज़ोर, जिससे गंभीर मुद्दे छिप जाते हैं।
– जनता की उदासीनता, जो भ्रष्ट नेताओं को सत्ता तक पहुँचने देती है।
समाधान की राह
गिरते स्तर को रोकने के लिए ठोस कदम जरूरी हैं।
– **चुनावी सुधार**: अपराधी पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के राजनीति में आने पर रोक और चुनावी खर्च की सीमा का कड़ाई से पालन।
– **संसदीय मर्यादा**: संसद और विधानसभाओं में आचरण के सख्त नियम और उल्लंघन करने पर दंड।
– **राजनीतिक शिक्षा**: जनता, विशेषकर युवाओं को राजनीति के आदर्श और मूल्यों से जोड़ना।
– **पारदर्शिता**: राजनीतिक दलों के वित्तीय स्रोत पारदर्शी हों और नेताओं की कार्यप्रणाली जनता के प्रति जवाबदेह हो।
– **आदर्श नेतृत्व को बढ़ावा**: राजनीतिक दल केवल चुनाव जीतने वाले चेहरों को नहीं, बल्कि ईमानदार और संवेदनशील व्यक्तियों को नेतृत्व दें।
निष्कर्ष
भारतीय लोकतंत्र की शक्ति उसकी संख्या नहीं, उसकी गुणवत्ता में निहित है। यदि जनता और नेता एक-दूसरे का भरोसा खो देंगे तो लोकतंत्र केवल कागज़ पर रह जाएगा। इसलिए राजनीति को पुनः सेवा और आदर्श का मंच बनाने की आवश्यकता है। नेताओं को यह समझना होगा कि कुर्सी स्थायी नहीं, पर उनकी नीयत और आचरण पीढ़ियों तक जनता के मन में दर्ज रहते हैं।
आज का समय आत्मचिंतन का है। यदि राजनीति का स्तर नहीं सुधरा तो लोकतंत्र का भविष्य संकट में पड़ सकता है। याद रखना होगा कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता के नेतृत्व में है, और नेतृत्व तभी महान बनता है, जब वह सेवा, नैतिकता और सत्य को अपने हृदय में धारण करे।
Politicianmirror.com के लिए भारत के राजनेताओं के गिरते स्तर पर प्रयागराज से अनीश कुमार सिंह का सम्पादकीय लेख
नेपाल का जनआंदोलन : सोशल मीडिया से शुरू, व्यवस्था परिवर्तन की मांग तक