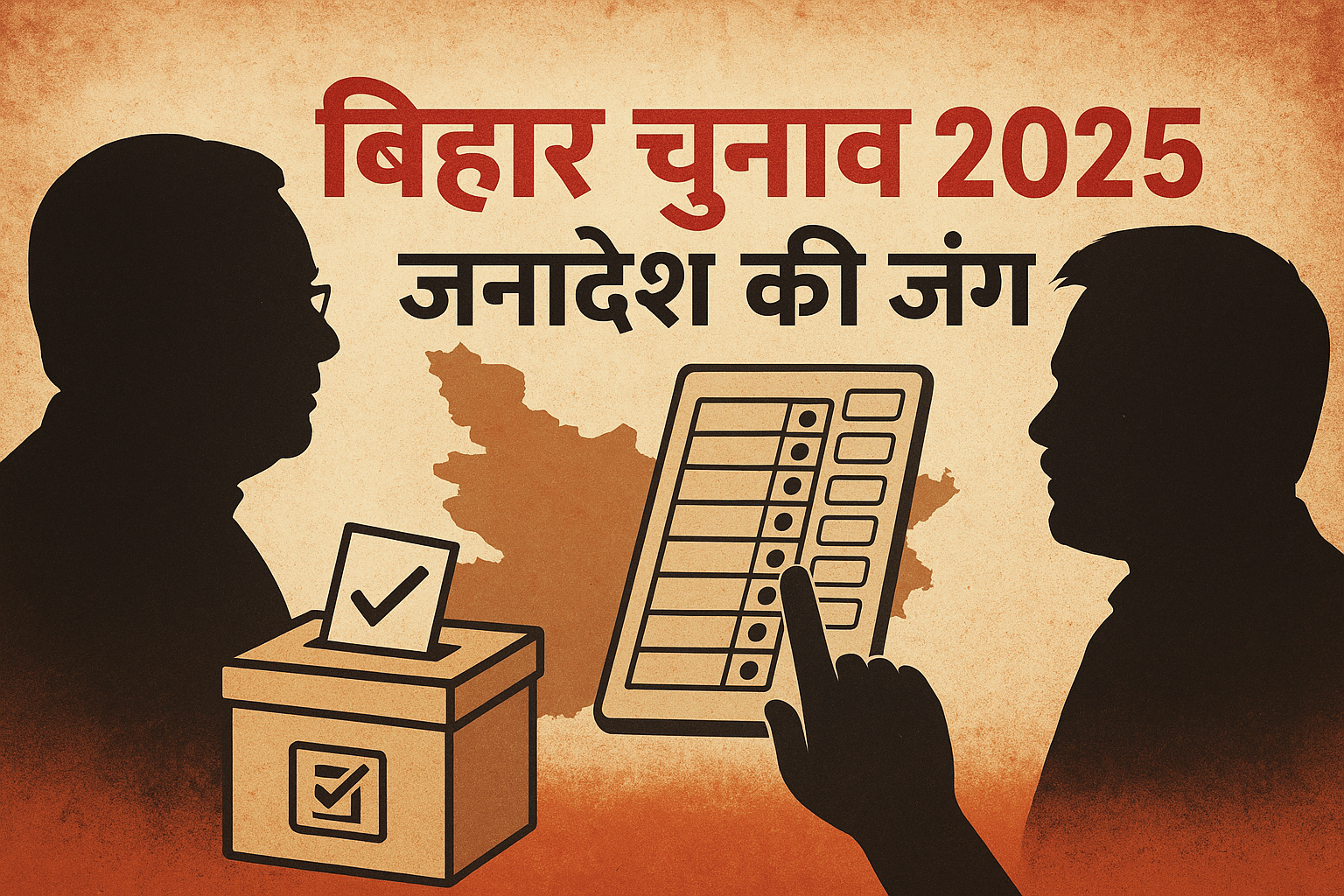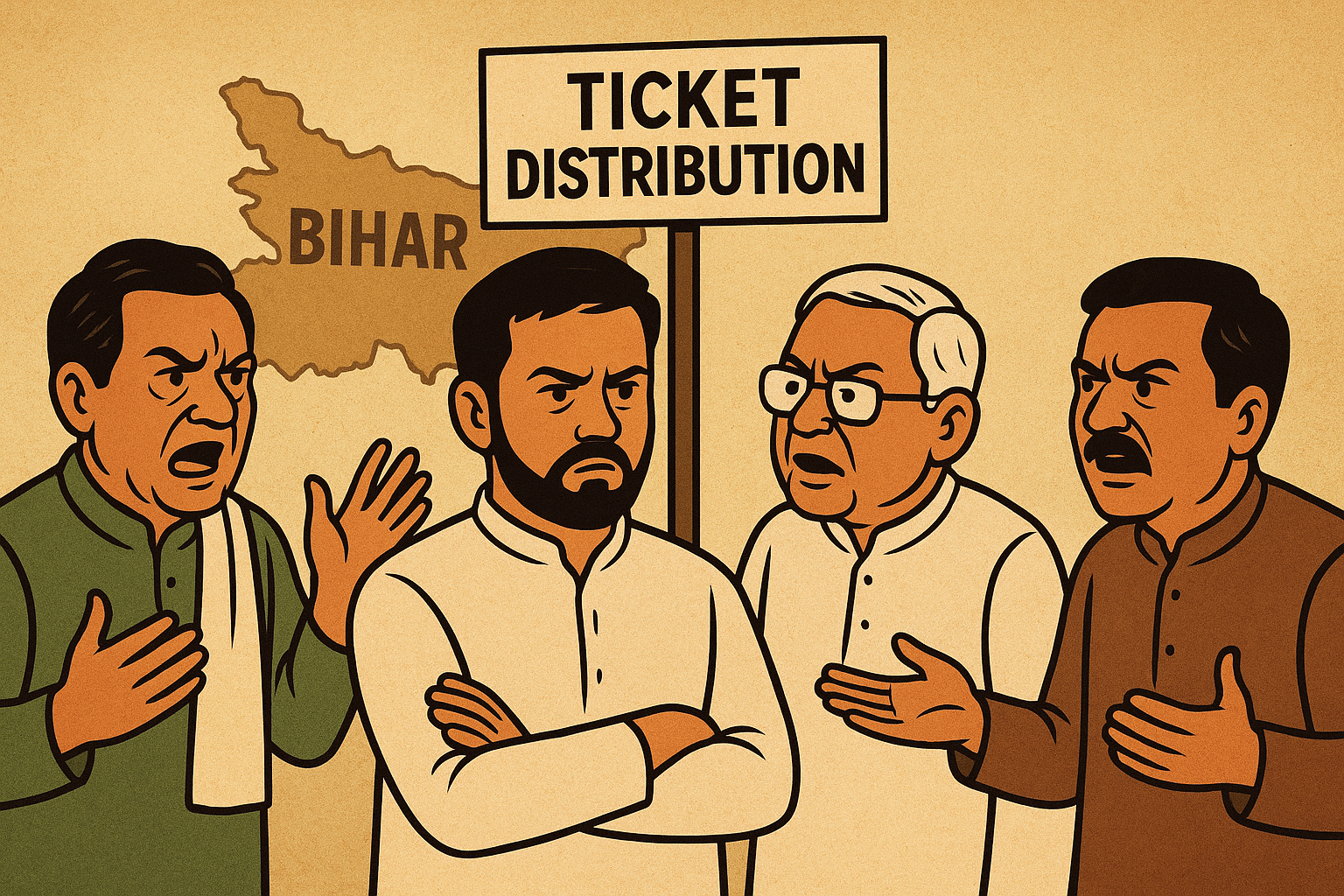सत्ता की चुप्पी और लोकतंत्र का मज़ाक
लोकतंत्र में जनता को यह भरोसा दिलाया जाता है कि उसका चुना हुआ प्रतिनिधि उसकी आवाज़ बनेगा। लेकिन यह भरोसा अक्सर टूट जाता है, जब वही नेता जो चुनावी मंचों से जनता के लिए जुझारू योद्धा बने नजर आते थे, सत्ता के सिंहासन पर बैठते ही “सत्ता की चुप्पी” का टैग ले लेता है।सत्ता के गलियारों में घूमते ये नेता ऐसे हो जाते हैं मानो उनके गले से स्वर-तंत्र निकालकर सरकारी अनुशासन लगा दिया गया हो।
नेता और सत्ता का रहस्यमयी परिवर्तन
अजब जादू है सत्ता का। विपक्ष में रहते हुए यही नेता रोज़ टीवी कैमरों के सामने नज़र आते थे, सरकार पर सवाल पूछते थे, आँकड़े गिनवाते थे, “जनता को इंसाफ़ चाहिए” चिल्लाते थे। लेकिन जैसे ही उनका दल सत्ता में आता है, अचानक ये वही नेता कहते दिखते हैं – “सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, जनता खुश है।”
यह रहस्यमय परिवर्तन क्या है? दरअसल, यह सत्ता के मोह, कुर्सी की गर्माहट और पद के आकर्षण का असर है। सत्ता चाहे कितनी भी जनविरोधी नीतियाँ लागू करे, अपने ही घर की कमियों को उजागर करना नेताओं को आत्महत्या जैसा लगता है। उन्हें डर लगता है कि अगर प्रश्न उठाए तो मंत्री पद छिन सकता है, अगला चुनाव टिकट कट सकता है या ‘उच्च नेतृत्व’ नाराज़ हो सकता है।
जनता के मुद्दे और नेताओं की चुप्पी
महँगाई की मार जनता झेल रही होती है, पेट्रोल-डीज़ल के दाम आसमान छूते हैं, दाल-रोटी तक आम आदमी की थाली से बाहर हो जाती है। लेकिन सत्ता में बैठे नेता कहते हैं – “महँगाई तो वैश्विक है।”
बेरोज़गारी चरम पर होती है, नौजवान दर-दर की ठोकरें खा रहा होता है। लेकिन सत्ता की गोदी में बैठे नेता कहते हैं – “आज युवाओं के पास स्टार्ट-अप के अवसर हैं, नौकरी की चिंता क्यों?”
स्वास्थ्य सेवाएँ चरमराती हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में दवाएँ नहीं। लेकिन नेता कहते हैं – “इतिहास में पहली बार इतना बड़ा सुधार हुआ है।”
यह तो वही बात हुई जैसी बच्चे को अधपकी खिचड़ी खिलाकर कहा जाए कि “बेटा, यह तो आधुनिक हेल्दी फूड है।” जनता समझती है कि यह झूठ है, लेकिन नेता फिर भी आत्म-प्रशंसा करते नहीं थकते।
लोकतंत्र का मज़ाक बनती सत्ता-भक्ति
लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा होती है कि सरकार की सही नीतियों का समर्थन और गलतियों पर करारा विरोध होना चाहिए। लेकिन जब सत्तापक्ष के नेता ही ताली बजाने तक सीमित हो जाते हैं, तो लोकतंत्र का चरित्र ध्वस्त हो जाता है। यह लोकतंत्र कम और दरबारी राजनीति ज़्यादा लगने लगता है।
इतिहास गवाह है कि जिन समाजों में सत्ता की आलोचना बंद हो जाती है, वहाँ तानाशाही जन्म लेती है। और आज के हालातों में वही दिखाई देने लगा है। संसद और विधानसभाओं में जनता की समस्याओं पर उतनी बहस नहीं होती जितना सरकार की उपलब्धियों के गीत गाए जाते हैं। कभी-कभी तो लगता है कि सत्ता का गुणगान करना ही सांसद/विधायक का असली काम है।
परिणाम और ख़तरे
इस प्रवृत्ति के भयानक परिणाम हैं:
- जनता का लोकतंत्र पर से भरोसा उठना शुरू हो जाता है।
- जनता का विश्वास टूटे तो सड़क पर आक्रोश का विस्फोट होना तय है।
- विपक्ष के कमजोर होने का फायदा यही सत्ता लेती है, और अंदर से उठती आवाज़ें भी दब जाती हैं।
- धीरे-धीरे नेताओं और जनता के बीच की खाई इतनी चौड़ी हो जाती है कि लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित रह जाता है।
सत्ता की चुप्पी तोड़ो
अगर देश को सचमुच मजबूत लोकतंत्र बनाना है तो सत्तापक्ष के नेताओं को हिम्मत दिखानी होगी। सवाल पूछना गुनाह नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। प्रत्येक नेता को यह याद रखना चाहिए कि उसने कसम जनता की खाई है, न कि कुर्सी की।
सच्चा नेता वही है जिसे जनता के दर्द को आवाज़ देने का साहस हो। आज ज़रूरत है उस साहस की—वरना आने वाली पीढ़ियाँ केवल यही कहेंगी:
“हमारे देश में नेता जनता के लिए नहीं, कुर्सी के लिए जन्म लेते हैं।”