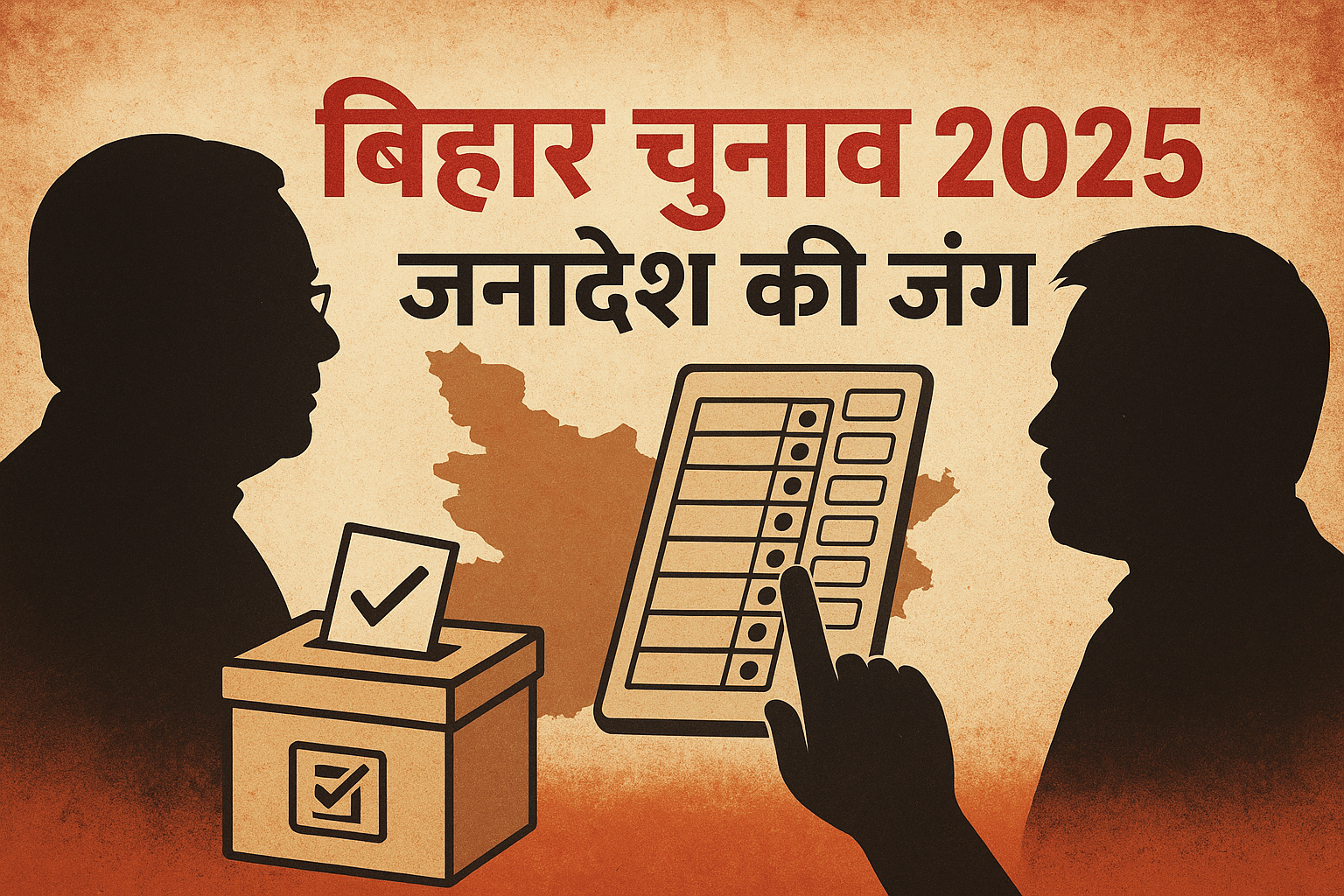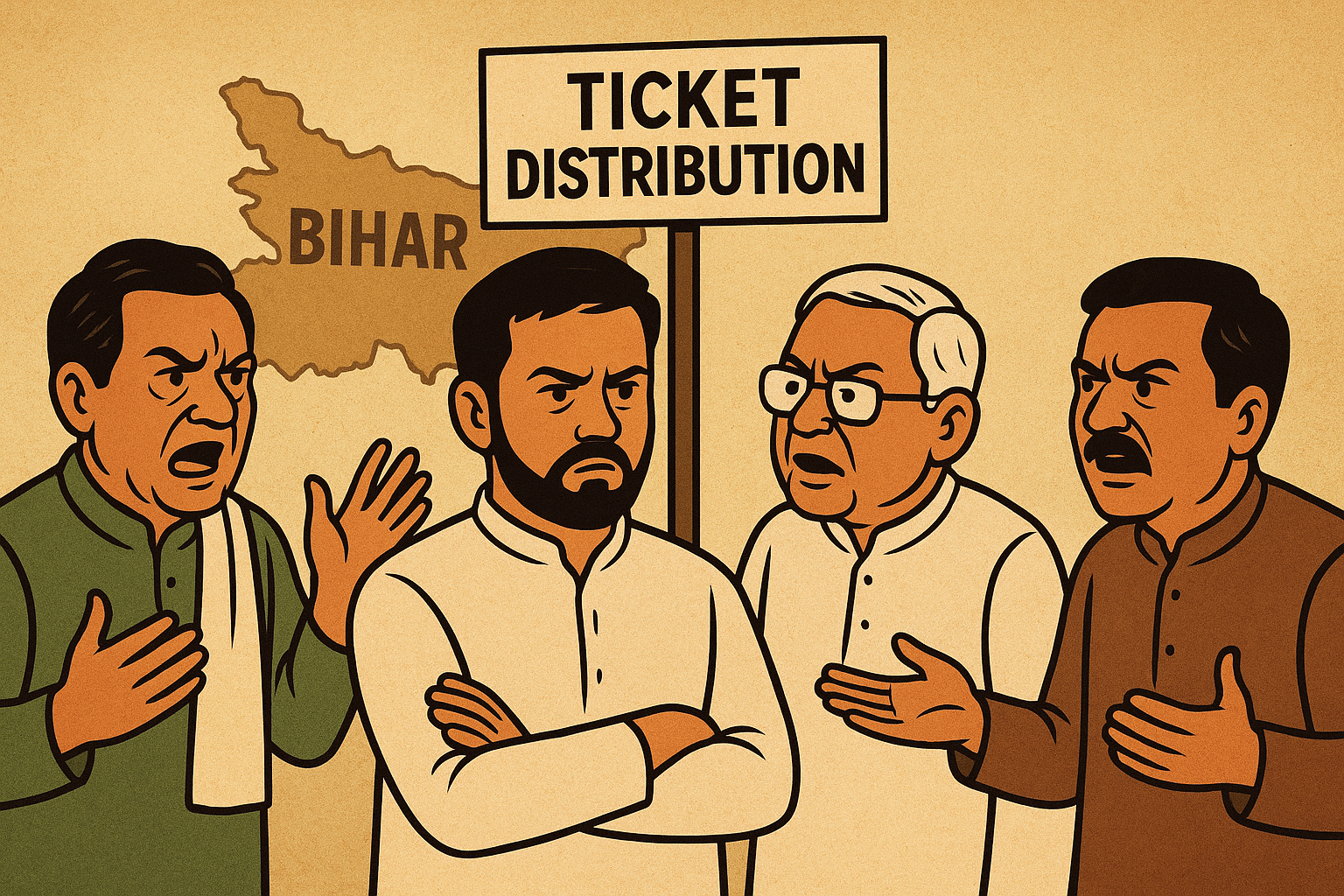भारत में जाति व्यवस्था एक प्राचीन सामाजिक संरचना है, जो कर्म और जन्म के आधार पर व्यक्तियों को वर्गीकृत करती है। यह व्यवस्था मुख्य रूप से हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था के रूप में विकसित हुई, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रमुख वर्ग हैं, लेकिन इसके अलावा अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) भी सामाजिक समूह बनाते हैं। जाति ने सामाजिक आदान-प्रदान, विवाह, खान-पान समेत अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया है।
जाति व्यवस्था ने समाज में एक स्थिर संरचना प्रदान की, लेकिन इसके कारण कई बार सामाजिक भेदभाव, असमानता और उत्पीड़न के मौके भी बढ़े। संविधान ने जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 17 के तहत अछूत प्रथा को निषेध किया और आरक्षण नीति लागू की, ताकि कमजोर वर्गों को समान अवसर मिल सके।
जाति का राजनीतिकरण और लोकतंत्र पर प्रभाव
जाति व्यवस्था का राजनीतिकरण भारत की स्वतंत्रता के बाद तेज गति से हुआ। राजनीतिक दल जाति समूहों को अपने वोट बैंक के रूप में देखते हैं, जिसके कारण जाति आधारित मतदान पैटर्न और राजनीतिक गठबंधन बड़ते गए। जाति आधारित राजनीति ने कई बार राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित किया है, लेकिन इसने कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों को राजनीतिक मंच भी दिया है।
जाति ने लोकतंत्र में सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को महत्वपूर्ण बनाया। दलित, ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए संगठित हुए, जिससे सामाजिक न्याय और समावेशी नीतियाँ बनीं। भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसे राजनीतिक दल अपने-अपने आधारों को जाति के हिसाब से मजबूत करने में लगे रहे हैं।
जातिगत राजनीति की सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका
जाति आधारित राजनीति ने कमजोर वर्गों की लड़ाई को सशक्त किया और उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने में योगदान दिया। यह पहचान और प्रतिनिधित्व की राजनीति है जिसने दलितों और पिछड़ों को सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल किया।
हालांकि, जातिगत राजनीति ने कई बार लोकतंत्र के आदर्शों को भी चुनौती दी। यह पहचान की राजनीति को बढ़ावा देती है, जिससे जातिगत विभाजन, बहिष्कार और स्थानीय विवाद जन्म लेते हैं। कई बार जाति के कारण राजनीतिक निर्णय समाज के व्यापक हितों से हटकर हो जाते हैं।
आरक्षण नीति और उसकी भूमिका
भारतीय संविधान ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था की है। यह नीति शिक्षा, सरकारी नौकरी, और संसद के लिए कोटा सिस्टम के रूप में लागू है। आरक्षण ने सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन में मदद की, लेकिन इससे विवाद और विरोध भी उत्पन्न हुए हैं।
आधुनिक भारत में जाति और राजनीति की परस्पर क्रिया
आधुनिक भारत में जाति और राजनीति का रिश्ता जटिल और गहरा हो गया है। राजनीति जाति को बदलती रहती है, तो जाति भी राजनीति को आकार देती है। राजनीतिक दल जाति-आधारित वोट बैंक के लिए रणनीति बनाते हैं, लेकिन जनतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना भी आवश्यक होता है।
जाति आधारित राजनीतिक पहचान समय-समय पर पुनः संरेखित होती है, जिससे नए राजनीतिक समीकरण बनते हैं। यह सामाजिक न्याय के लिए सकारात्मक है, मगर इसे लोकतंत्र के व्यापक हित में संतुलित करके चलना चुनौतीपूर्ण है।
इस प्रकार, भारत की जाति व्यवस्था न केवल एक सामाजिक संस्था है, बल्कि इसका राजनीति पर गहरा प्रभाव है। यह देश की राजनीतिक संस्कृति, सामाजिक न्याय, और चुनावी राजनीति को प्रभावित करती है। जाति आधारित राजनीति की समृद्ध परंपरा के साथ, इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आयामों को समझकर ही भारत के लोकतंत्र को सतत विकास की ओर ले जाना संभव है।

Politicianmirror.com के लिए भारत की जाति व्वस्था पर सम्पादकीय लेख